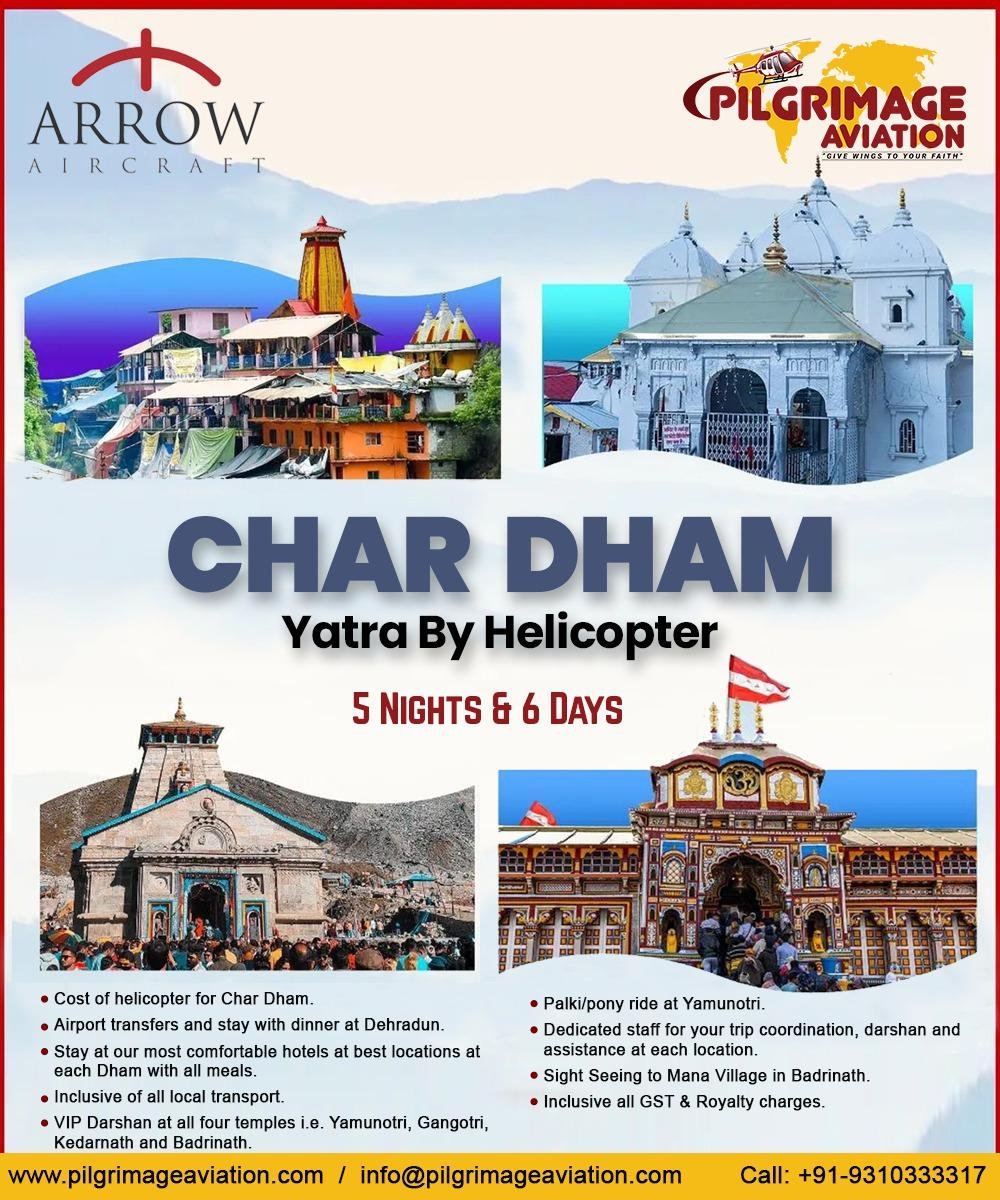पिछले कई दशकों से महिला सशक्तिकरण एक ऐसा सर्वव्यापी विषय बन चुका है जिस पर सामान्य से लेकर विशिष्ट, यहाँ तक कि अतिविशिष्ट वर्ग भी समय-समय पर अपना दृष्टिकोण सामने रखता आया है। आज महिला सशक्तिकरण के लिए एक अभियान सा चल रहा है, लेकिन ग़ौर से देखा जाए तो इस अभियान के क़दम कई बार डगमगाते से लगते हैं। कहीं छिटपुट सफलताएं मिल भी जाएं किन्तु एक निश्चित लक्ष्य नज़र नहीं आता। वैसे इस सम्बन्ध में क़ानून ने भी ख़ुद को बदला है, अनेक संशोधन हुए हैं। आज प्रशासन कमर कसकर तैयार नज़र आता है, लेकिन समस्या जैसी की तैसी है। असल मुद्दा सिर्फ कमज़ोर को ताक़त देने तक नहीं सिमटा है बल्कि लड़ाई उस लिंग भेद को मिटाने की है जो सदियों से जड़ें जमाये बैठा है।
उन अधिकारों को वापस पाने की है जो सृष्टि की शुरुआत से नारी को मिले थे। जब मातृ सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे, तब घरों की चारदीवारियों का आविष्कार नहीं हुआ था। खुले आसमान तले, प्रकृति के संसर्ग में कहीं नदी किनारे तो कहीं घाटियों में बसे इन कुनबों की मुखिया एक स्त्री हुआ करती थी। प्राकृतिक आपदाएं आयें या हिंसक पशुओं का आक्रमण हो, अपनी मुखिया के साथ मिलकर पूरा कुनबा उस विपत्ति का सामना करता। एक दूसरे की शक्तियों को सराहकर, मिलकर काम करने की इसी खूबी के चलते सभ्यता का विकास हुआ। घर बने, समाज बना और पुरुष का वर्चस्व हावी होता गया। जो नारी प्रकृति इष्ट देवों की साधना कर अपने कुनबे की मंगलकामना करती थी, उसी की सहनशक्ति को भुनाने के लिए पुरुषों ने कुछ खास दिन बना लिये, अपने लिए।
स्त्री को भूखे रहकर उन ख़ास दिनों के आयोजन और व्रत-उपवासों की ज़िम्मेदारी ओढ़ाकर, पुरुष निश्चिन्त हो गया। पूजा विधानों से, धार्मिक ग्रंथों से स्त्री को दूर कर दिया गया। फिर एक-एक कर पुरुष ने उसके सभी अधिकार लेने शुरू कर दिये और धीरे-धीरे नारी नेपथ्य में सिर्प उपभोग की वस्तु बनती गयी। वो तमाम परम्पराएं भी लुप्त होती गयीं जो नारी को समान स्थान देने के लिए बनायी गयी थीं। स्वयंवर प्रथा द्वारा अपना वर स्वयं चुनने वाली नारी, अगर आज के दौर में ऐसी हिमाकत कर बैठे तो उसका सर क़लम करने के लिए उसके पिता-भाई खड़े हो जाएंगे। खाप पंचायतें बैठ जाएँगी। आज के दौर में इसी मानसिकता के चलते कई प्रदेशों में बेटियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है।
स्त्री का जीवन सहज-सरल नहीं, ये मुश्किलें खुद पुरुषों द्वारा ही खड़ी की जाती हैं और मजे की बात ये कि उनसे जूझती स्त्री के प्रति पुरुष सहानुभूति जताने भी आ जाता है और उसे अबला का एक और ख़िताब दे जाता है। यह अबला जब सबला बन जाये तो पुरुष को बर्दाश्त नहीं होता। एक उच्च शिक्षण संस्थान में आयोजित समूह प्रतियोगता के दौरान मुखिया ने एक लड़की को हटाकर एक ऐसे लड़के को मुख्य दायित्व सौंप दिया, जो टीम संचालन और अच्छे प्रदर्शन में कहीं पीछे था। तर्क था, `वो लड़का है सँभाल लेगा, तुम नहीं कर पाओगी।’ अगर यह `न कर पाने वाली स्त्री अगर ग़लती से अपनी योग्यता दिखा दे तो पुरुष तिलमिला उठता है।
एक कार्यालय में पदोन्नति के लिए दिये गये एक ज़रूरी प्रोजेक्ट में जब एक पुरुष सहकर्मी पिछड़ने लगा तब उसने अपनी महिला सहकर्मी की पूरी रिपोर्ट ग़ायब कर दी और सबने उसकी बात पर ही विश्वास कर मान लिया कि वो स्त्री अपनी रिपोर्ट ग़ायब होने की मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। स्त्री की योग्यताओं के आँकलन की जब भी बात आती है, पुरुष मानसिकता उधड़ने लगती है। अगर स्त्री योग्य है, तो उसे पीछे खींचने के लिए मानसिक और शारीरिक शोषण जैसे अस्त्र धड़ल्ले से इस्तेमाल किये जाते हैं। वो न माने तो उस पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है।
ये अपाला, गार्गी, रानी लक्ष्मीबाई, साक्षी मलिक, दीपा करमाकर और इन जैसी तमाम स्त्रियों का देश है। यहाँ महिला सशक्तिकरण का अभियान अगर स्त्रियों के पोशाकों के चुनाव तक सिमट गया, मासिक धर्म के दौरान धार्मिक स्थलों में प्रवेश की बहस में उलझ गया तो, ऐसे ही परिणाम निकलते रहेंगे। इस लड़ाई में अपना पक्ष रखने के लिए स्त्री को भी यह समझना होगा कि वो सास, जेठानी, माँ होने से पहले स्त्री है, उसे दूसरी स्त्री का मन समझना होगा। स्त्री तो स्वयं शक्ति है। उसे सिर्फ अपने वो अधिकार स्वतंत्र कराने हैं, जिन पर सामाजिक और मानसिक ताले जड़े गये हैं। इस लड़ाई में उसे थोड़ी समझदारी और सहयोग की अपेक्षा है उन सभी पुरुषों से, जो उसके जीवन आकाश में सहभागी बनते हैं।
– राजुल