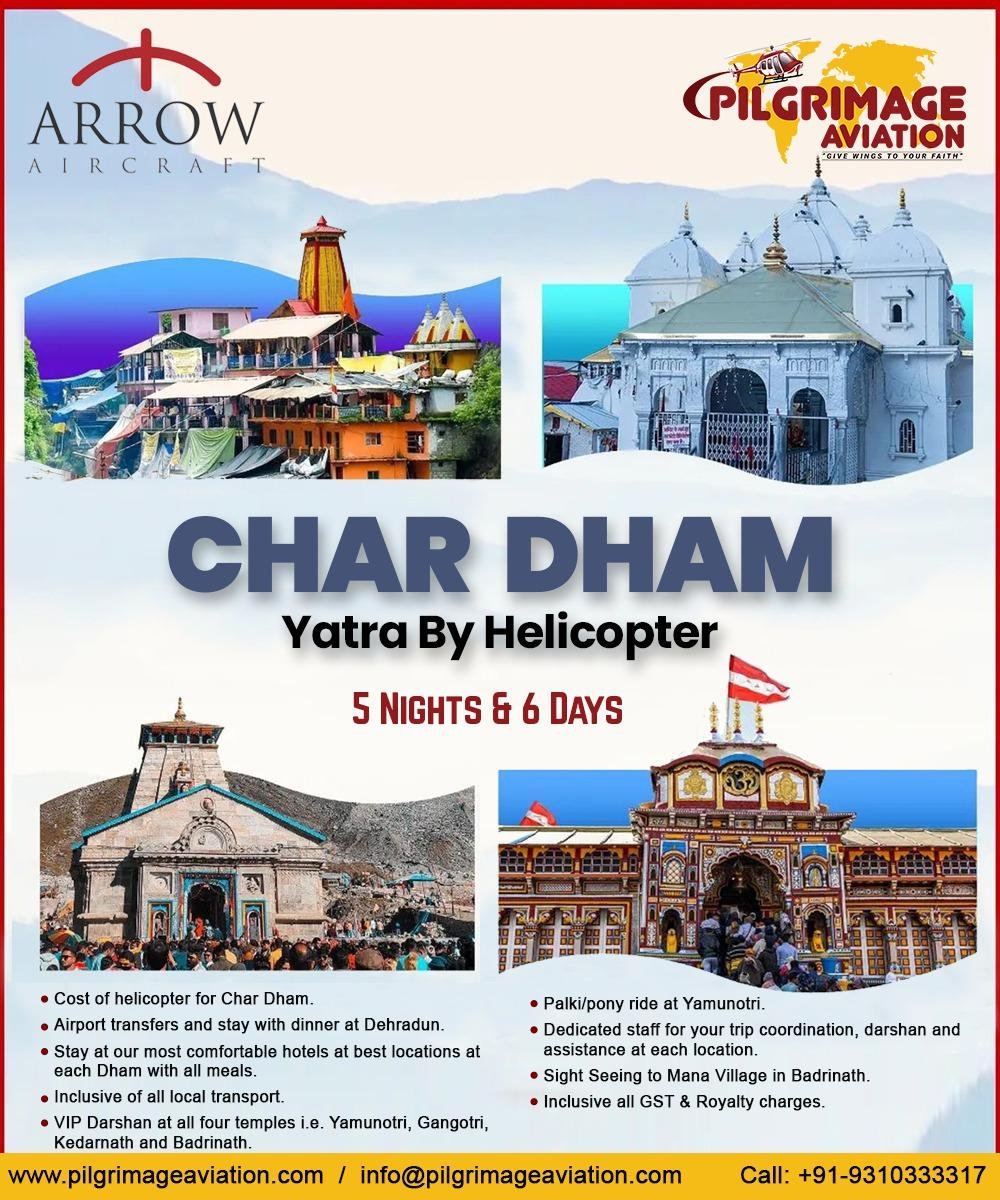आलोचना अब एक ख़तरनाक काम है. इसका एहसास मुझे हाल में तब हुआ जब मैंने मैसूर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के प्राध्यापक बीपी महेशचंद्र गुरु की गिरफ़्तारी की आलोचना की. इस आलोचना के तत्काल बाद कई लोग यह बताने वाले निकल आए कि इस गिरफ़्तारी के लिए मोदी सरकार ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है. हालांकि वे यह छुपा गए कि पुलिस में उनकी शिकायत एक अल्पज्ञात हिंदू संगठन ने की थी. कुछ लोगों ने इस बात के लिए भी मेरी भर्त्सना की कि मैंने अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में गुरु के दलित होने का उल्लेख किया और इसे भी उनकी गिरफ़्तारी की एक वजह के तौर पर रेखांकित किया.
क्या यह बात महत्त्वपूर्ण है कि महेशचंद्र गुरु की गिरफ़्तारी मोदी सरकार ने नहीं, किसी और सरकार ने की है? अभिव्यक्ति के ख़तरों के प्रति संवेदनशील हम लोग यह जानते हैं कि कोई भी सरकार किसी भी तरह के वैचारिक प्रतिरोध, या असहमति या किसी असुविधाजनक विचार को सहने को तैयार नहीं होती. वह ऐसे विचारों को भी रोकती है जिनसे उसके अलोकप्रिय होने का खतरा हो- चाहे वे विचार कितने भी सही हों. इस मायने में कांग्रेसी सरकारों का अनुभव भाजपा सरकारों के अनुभव से कहीं बेहतर नहीं रहा है. कांग्रेस ने भी कई किताबों को प्रतिबंधित किया है- कई लेखकों को उत्पीड़ित किया है. बौद्धिक दमन का मार्क्सवादियों का इतिहास तो कहीं ज्यादा रक्ताक्त रहा है. नक्सलियों के ख़िलाफ ग्रीन हंट जैसे ऑपरेशन चलाने में चिदंबरम-मनमोहन या मोदी-राजनाथ में कोई अंतर नहीं है.
जब मार्क्सवादियों ने नक्सलबाड़ी से उठे आंदोलन को कुचला तो उसकी बड़ी तीखी आलोचना हुई. भारतीय साहित्य में एक पूरी पीढ़ी नक्सलवाद की वैचारिक सहानुभूति के बीच बड़ी हुई और उसने पिट रहे, मारे जा रहे लोगों का साथ दिया. कांग्रेस ने जब किताबों को प्रतिबंधित किया या लेखकों को तंग किया, तब भी उसकी आलोचना हुई. इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस का चाबुक सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व पर ही नहीं, लेखकों-पत्रकारों पर भी चला और कई ने 19 महीने की पूरी जेल काटी. राजीव गांधी ने जब प्रेस बिल लाने की कोशिश की तो उसका इतना तीखा विरोध हुआ कि राजीव गांधी ने क़दम पीछे खींच लिए. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या भी कांग्रेस के समय ही हुई और उस समय भी उसके प्रति पूरा बौद्धिक आक्रोश फूटा. मनमोहन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उसकी भी भरपूर खिल्ली उड़ाई गई. सिंगुर और नंदीग्राम में सीपीएम के दमन के ख़िलाफ़ लेखक और संस्कृतिकर्मी सड़क पर उतरे.
मगर यह पहली बार है जब लेखक की गिरफ़्तारी का विरोध करने पर आप पर हमला हो सकता है. यह कहा जा सकता है कि इसके लिए अमुक सरकार ज़िम्मेदार है और अमुक सरकार नहीं. याद कर सकते हैं कि कर्नाटक के लेखक एमएम कलबुर्गी की हत्या का विरोध कर रहे लोगों को बार-बार याद दिलाया गया कि यह हत्या तो कर्नाटक में हुई है, जहां कांग्रेस की ही सरकार है. यही नहीं, इस दौर में, विचार-विमर्श और तर्क के नाम पर एक नई तरह की छींटाकशी भी दिख रही है. लगभग हर मुद्दे पर कोई पूछने चला आता है कि किसी लेखक ने अपने पुरस्कार वापस किए या नहीं. जिन लेखकों को आप पढ़ने तक की जहमत नहीं उठाते, जिनके बारे में आपकी कोई राय नहीं है, जिनकी किताबें बिकती नहीं, उन मामूली से लोगों की पुरस्कार वापसी के उद्यम पर आप इतने नाराज़ हैं कि इसके पीछे संगठन की ताकत और साज़िश की नीयत देख रहे हैं. यह मानने को तैयार नहीं हैं कि लेखकों ने अपने प्रतिरोध का बहुत ही लोकतांत्रिक तरीक़ा चुना था जिससे किसी के अधिकारों की हानि नहीं होती थी. बेशक, इस प्रवृत्ति में कुछ भेड़चाल रही होगी, और संभव है, कुछ के भीतर इससे हासिल यशकामना भी हो, लेकिन सच यह है कि अंततः इसके पीछे भी लेखकीय स्वाभिमान की भावना ही थी. वरना इस दौर में चापलूसी और समर्थन से पुरस्कार, यश, और पद तीनों हासिल हो रहे हैं- पुणे फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट से लेकर निफ्ट और दूसरी संस्थाओं में हो रही भर्तियां यही बताती हैं. हालांकि खतरा फिर यही है- लोग पूछने लगेंगे कि कांग्रेस के समय कैसे लोगों की भर्ती होती थी? उन्हें कौन याद दिलाए कि कांग्रेस के समय भी ऐसे लोगों की आलोचना होती थी.
बहरहाल, आलोचना के प्रति इस उद्धत और आक्रामक रुख़ की वजह क्या है? एक वजह तो उस अनपढ़ता और स्मृतिविपन्नता में छुपी है जो हमारे समाज में लगातार बढ़ रही है. लोग न इतिहास से परिचित हैं न परंपरा से. न समाज को समझते हैं न संवाद को. वे अपने आसपास के हालात भी देखने को तैयार नहीं हैं. बेशक, इस बढ़ते हुए सतहीपन को, इस लगातार छिछले होते समय को हमारी संसदीय राजनीति के विद्रूप ने भी बढ़ावा दिया है, और इस विद्रूप की वजह से ख़ुद वह संसदीय लोकतंत्र संदिग्ध हुआ है जिसमें सामाजिक न्याय और बराबरी की कहीं ज़्यादा गुंजाइश होती है. लेकिन जो लोग इस विद्रूप के सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, वही विकास की भाषा बोलते एक फासीवाद की अभ्यर्थना में खड़े हैं. उन्हें यह मंज़ूर नहीं कि कोई न्याय का प्रश्न उठाए, कोई याद दिलाए कि विकास के इस दावे में छेद हैं, कोई बताए कि इस देश में बोलने की आज़ादी वह चीज़ है जो इसके लोकतंत्र को उसकी बहुत सारी कमियों के बावजूद अद्वितीय और संभावनापूर्ण बनाती है, कोई कहे कि धर्म और राष्ट्र के नाम पर झूठ नहीं बोने जाने चाहिए, उन्माद नहीं फैलाया जाना चाहिए, कोई सोचे कि विचार के दायरे में धर्म और राष्ट्र की नई व्याख्याएं भी आती हैं जो जनोन्मुख चेतना के पोषण में सहायक होती हैं.
उल्टे ये लोग यह भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि गरीबी भले बनी रहे, बेरोज़गारी भले बची रहे, औरतें भले उत्पीड़ित होती रहें, दलित और आदिवासी भले पिटते रहें, धर्म और राष्ट्र का अभिमान सबसे बड़ी चीज़ है और इसी में उनका स्वप्न, उनकी मुक्ति निहित है. कहने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे लोगों को सरकार की आलोचना राष्ट्र की आलोचना लगती है, प्रधानमंत्री को प्रश्नांकित करना देशद्रोह लगता है और धर्म की पुनर्व्याख्या की कोशिश करना पूरी सभ्यता के लिए ख़तरनाक लगता है. वे देश और समाज को जीवंत वाद-विवाद और संवाद की हलचल से बनते देखना नहीं चाहते, वे ऐसे लेखक, कलाकार और बौद्धिक नहीं चाहते जो किसी को प्रश्नांकित करें.
लेकिन हमें यह करते रहना होगा. अपनी आलोचना पर छींटाकशी झेलते हुए भी, अपने तुच्छ लेखन और तुच्छतम पुरस्कारों को ग्रहण करते या छोड़ते हुए भी, हमें याद दिलाना होगा कि किसी भी जीवित समाज में उसका लेखक, संस्कृतिकर्मी या बौद्धिक सिर्फ एक विपक्ष की भूमिका में ही रह सकता है. लेखक विचारधाराओं के दुर्गों का प्रहरी नहीं होता, वह उनकी दरारें खोजने वाला सेंधमार होता है- ग्राहम ग्रीन ने कहा था कि उसे चोर और तस्कर की तरह दबे पांव इन दुर्गों में दाखिल होना पड़ता है.
जब 1998 में वाजपेयी सरकार ने ऐटमी परीक्षण किए थे, तब हमने उनकी निंदा की थी, जब मनमोहन सिंह ने अमेरिका से ऐटमी करार किया तब हमने उनकी आलोचना की और अब जब नरेंद्र मोदी एनएसजी की सदस्यता के लिए बाल हठ लगाए दुनिया भर का निष्फल भ्रमण कर रहे थे, तब हम उसे उपहास से देखने को स्वतंत्र हैं. जब नरसिंह राव सरकार के समय बाज़ार खोले गए, तब भी बहुत सारे लेखकों और बुद्धिजीवियों ने उसे गलत बताया, जब कांग्रेस के समय ख़ुदरा कारोबार में सौ फीसदी निवेश का प्रस्ताव आया तब भी इसकी जमकर आलोचना हुई और जब नरेंद्र मोदी की सरकार सारे क्षेत्रों में विदेशी पूंजी को बढ़ावा दे रही है तो दरअसल यह भाजपा है जो अपनी वैचारिकी से विश्वासघात कर रही है, लेखक और पत्रकार नहीं हैं जो अपना पक्ष भूल रहे हैं.
साठ, सत्तर और अस्सी के दशकों में रांची, मेरठ, मलियाना, जमशेदपुर, बिहार शरीफ़, भागलपुर या दूसरी जगहों पर हुए दंगे हों, 1984 की हिंसा हो, बाबरी मस्जिद ध्वंस के पहले और बाद के उन्माद में हुई हिंसा हो, 2002 की गुजरात की प्रायोजित हिंसा हो, मुजफ़्फ़रनगर और बरेली के दंगे हों या संगीतकारों की भूमि कैराना को सांप्रदायिक जहर से सींचने की साज़िश हो- लेखक और पत्रकार हमेशा से इन सबके ख़िलाफ़ लिखते और बोलते रहे हैं- राजनीतिक दलों ने बेशक इन सब पर पाले बदले हों. तो अपने ऊपर हो रही छींटाकशी के बावजूद हमें बोलते रहना होगा. ये हम तय करेंगे कि कब लिखेंगे, कब जुलूस निकालेंगे, कब पुरस्कार लौटाएंगे और कब विरोध का कोई और तरीका चुनेंगे. बेशक ऐसी काली भेड़ें हर दौर में रही हैं जो सत्ता प्रतिष्ठानों के साथ चलती रही हैं. अभी वे कुछ बढ़ गई हैं और बिल्कुल राजनीतिक प्रवक्ताओं में बदल गई हैं. इन पर बस तरस खाया जा सकता है.
और जहां तक किसी की गिरफ्तारी को जाति से जोड़ कर देखने का सवाल है, कृपया भारतीय जेलों में बंद विचाराधीन और सज़ायाफ्ता कैदियों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन कर लें- सच्चाई सामने आ जाएगी. हमारी जेलों में बंद आधे से ज़्यादा लोग मुस्लिम, दलित और आदिवासी हैं. या तो ये मान लें कि ये अपराधी लोग हैं या फिर यह समझने की कोशिश करें कि हमारी व्यवस्था इन वर्गों के साथ एक अन्याय कर रही है. अगर इतना सब्र न हो तो यहां भी छींटाकशी कर लें. आखिर लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी छींटाकशी करने वालों को भी मिलनी चाहिए. खतरनाक बात बस इतनी है कि यह छींटाकशी करने वाले लोग अंततः उन गिरोहों के साथ खड़े नज़र आते हैं जो कभी किसी को गोली मारते हैं, कभी किसी के चेहरे पर कालिख पोतते हैं, कभी किसी के ख़िलाफ पुलिस स्टेशन जाकर झूठी शिकायत दर्ज कराते हैं और कुल मिलाकर भय का वह माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी असहमति जताते हुए डरे.