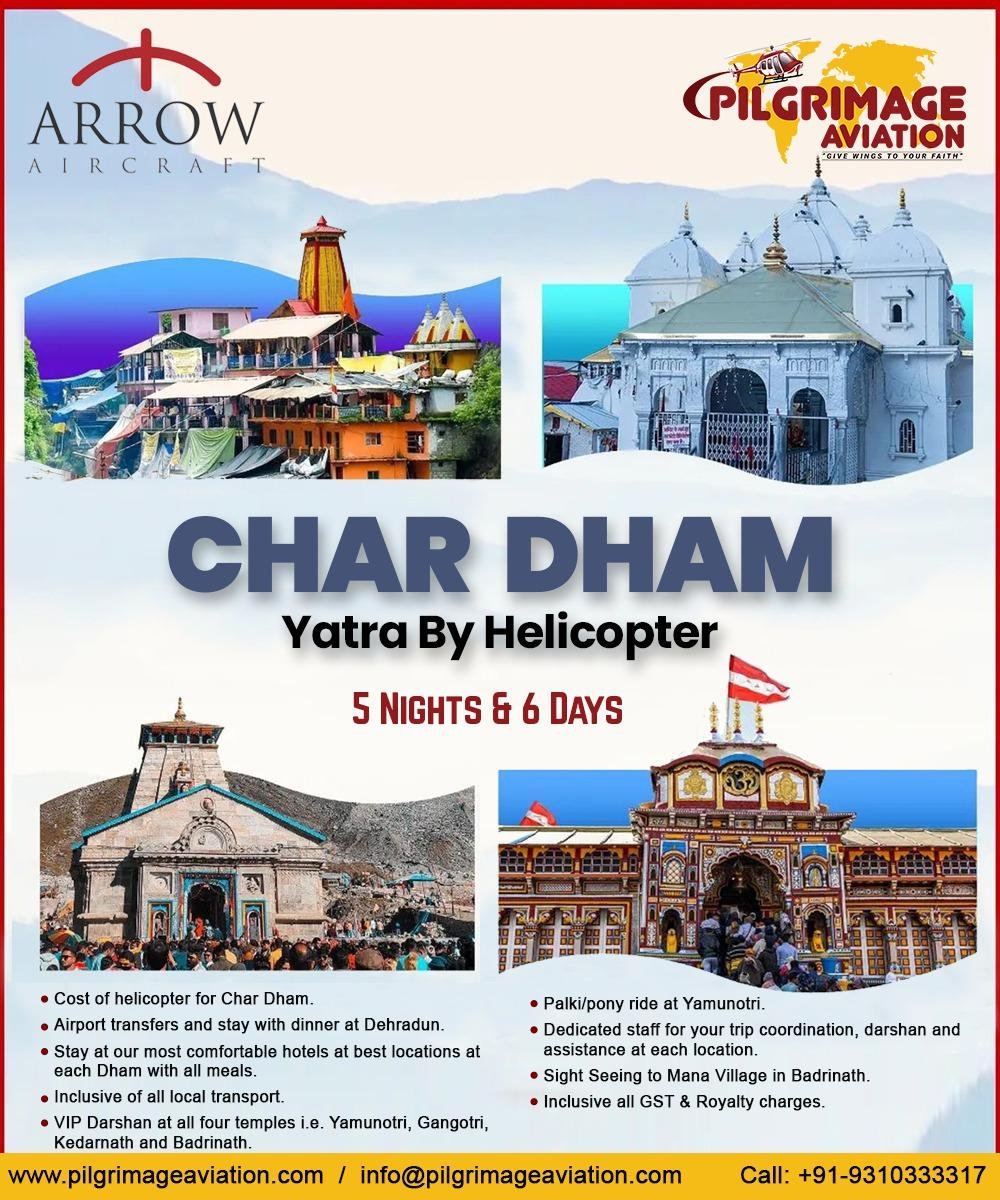आज से लगभग सौ साल पहले स्त्री-शिक्षा के नाम पर स्त्री-सुबोधिनी बाँच लेने की योग्यता पर्याप्त समझी जाती थी। स्त्री सुबोधिनी बाँचने की योग्यता इसलिए कि समाज में नारी ‘पदार्थ’ बनी रहकर अपना पारिवारिक दायित्व भली-भाँति सँभाल सके। घर की चार दीवारी से बाहर निकल खुली हवा में साँस ले पाना उसके लिए आकाश-कुसुम तोड़ लाने जैसा था। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जमाने की स्त्रियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जब उनके परिवार की स्त्रियाँ गंगा स्नान के लिए लालायित होती थीं तो नौकर उन्हें नदी में पालकी समेत डुबकी लगवा देते थे। उस जमाने की औसत स्त्री के बारे में ‘सीमोन द बोउवा’ ने लिखा है कि वह गाय की तरह किसी घर के अन्दर रँभाती हैं और बछड़े के बदले घास का पुतला थनों से सटाये कातर होकर दूध देती हैं।’
उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में एक छोटा सा शहर है बलिया। वहाँ की स्त्रियों की दशा वैसी ही थी, जैसी भारत के अन्य भागों में, विश्व के किसी कोने में। उन्हें समुचित शिक्षा मिले, इसके बारे में गंभीरता से किसी ने सोचने-विचारने की जरूरत एक लम्बे समय तक नहीं समझा। आवश्यकता ही क्या थी। बालिका एक चौखट के अन्दर जन्म ले और विवाह के बाद दूसरी चौखट के अन्दर दाखिल हो, जहाँ कर्तव्यों के पुलिंदों के बीच दबती पिसती स्वयं को होम करती चले, मरने पर पति या पुत्र का कन्धा-भर मिल जाये, इससे अधिक की बात ही कहाँ उठती थी!
लेकिन उसी पिछड़े शहर में बड़ी-बड़ी आंखों, गर्दन तक फैले लंबे कान और तीखे नाक नक्श की एक युवती को अपना वजूद तलाशने का मौका मिला। ‘दु:ख मनुष्य को माँजता है’ कहावत उन पर शब्दश: लागू हुई। विवाह के बाद उन्होंने जिस घर में प्रवेश किया, वह जमीदारी ठाट-बाट का घर था। उनके पति श्री महादेव भगत एक खाते-पीते जमीदार थे। लेकिन विरासत में उन्हें जो जमींदारी मिली थी, वह दुर्भाग्यवश हाथ से निकल गयी। वैवाहिक जीवन शुरू होते ही नियति ने उन्हें संघर्ष के रास्ते पर खड़ा कर दिया।
जमींदारी के तौर-तरीकों से बाहर निकलने में भगतजी को थोड़ा वक्त लगा। आस-पड़ोस के लोग उनकी बड़ी इ़़ज्जत करते थे। लोगों की समस्याओं के निदान के लिए उनके पास तुलसी और रहीम के दोहों का खजाना था। उनके उपदेशात्मक दोहों के लोग बड़े कायल थे। बुरा समय आने पर पत्नी को दोहों के माध्यम से मौखिक सांत्त्वना देते देते एक दिन वे अचानक कह बैठे- ‘‘लक्ष्मी! तुम पढ़ाई करो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची शिक्षित बने। तुम शिक्षा प्राप्त करोगी तो हमारे बच्चे भी अनपढ़ नहीं रह पायेंगे।’’ लक्ष्मी देवी स्तब्ध थीं कि पति स्वयं अनपढ़ हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाई-लिखाई का आदेश दे रहे हैं। उन्होंने सोचा, थोड़े ही दिनों में भगतजी का जोश ठंडा हो जायेगा। लेकिन भगतजी जिस बात के लिए तुल गये, वह बात तो पत्थर की लकीर साबित हुई वे लड़कों के स्कूल में जाकर हेडमास्टर से मिले और उनकी सहायता से उन्होंने किताब-कॉपी की व्यवस्था की।
उसी स्कूल के किसी शिक्षक की सहायता से लक्ष्मी देवी ने पढ़ाई-लिखाई शुरू की। उनकी कठिनाई हल करते के लिए गुरूजी भगतजी की उपस्थिति में हर संभव सहायता करने लगे। लक्ष्मी देवी ने अपर मिड़िल की परीक्षा प्राइवेट विद्यार्थी की हैसियत से दी। उनकी मेहनत और भगतजी की प्रेरणा रंग लायी। वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गयीं। यह खबर शहर में आग की तरह फ़ैल गयी। जिसे देखो, वही कहता फिरता, लक्ष्मी देवी पास हो गयीं। बलिया शहर में एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया और लक्ष्मी देवी का अभिनन्दन किया गया। दो शब्द बोलने के लिए वे मंच पर खड़ी हुईं तो उन्होंने रूँधे हुए स्वर से स्वीकार किया कि ‘‘मेरे पति के हाथ से जमींदारी का निकल जाना ही मेरी शिक्षा-दीक्षा का सबब बना। मुसीबत ने ही मेरे पति को रोशनी दिखायी।’’ शिक्षा के तेज ने जमींदारी के वैभव को फीका साबित कर दिया।
शहर की एक स्त्री यदि शिक्षित हो सकती है तो दूसरी बालिकाएँ क्यों नहीं? यह सवाल शहर के बुद्धिजीवियों को कुरेदने लगा। प्रश्न विकट था, क्योंकि बिना बालिका विद्यालय के शहर की बालिकाएँ शिक्षित होतीं भी तो कैसे! इसलिए शहर के धनी-मानी लोगों ने सरकार से स्कूल खोलने की बार-बार अपील की। सब लोग समझते थे कि स्कूल के लिए केवल ईंट-गारे का ढाँचा ही पर्याप्त नहीं होता, इसके लिए जरूरी थी कम-से-कम एक अदद शिक्षिका। शिक्षिका का बन्दोबस्त तभी हो सकता था, जब शहर की एक मात्र शिक्षित महिला लक्ष्मी देवी स्कूल में पढ़ाने का उत्तरदायित्व सँभालतीं। यदि वे तैयार हो भी जाती तो क्या उनके पति भगतजी इसके लिए अनुमति देते?
हुआ वही, जिस बात का डर था। इलाहाबाद की शिक्षा-निर्देशिका सुची गाँधी (स्वर्गीय श्री फ़िरोज गाँधी की सगी बहन) ने अपना एक प्रतिनिधि-मण्डल बलिया भेजा, जिसके सदस्यों ने लक्ष्मी देवी और उनके पति भगतजी से मुलाकात की कोशिश की। भगतजी ने प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों को यह कहकर अपने दरवा़जे से ही भगा दिया कि आप लोगों का दिमा़ग तो खराब नहीं हो गया है? मेरी पत्नी शिक्षित है सही, पर मैं उसे नौकरी करते की इजा़जत कैसे दे सकता हूँ!
प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य निराश हो वापस लौट गये, लेकिन सुश्री गाँधी ने तय कर लिया था कि बलिया में सरकारी बालिका विद्यालय खुलेगा और उसकी प्रधानाध्यापिका का पद-भार लक्ष्मी देवी ही ग्रहण करेंगी। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने फिर एक दूसरा प्रतिनिधि-मण्डल बलिया भेजा। इस बार भी उसके सदस्यों को बैरंग वापस लौटता पड़ा। श्री महादेव भगत के गले के नीचे यह बात उतर ही नहीं पा रही थी कि उनकी पत्नी नौकरी करे। इसके साथ ही एक बात और उन्हें परेशान कर रही थी कि लक्ष्मी देवी ने शिक्षा ग्रहण की है, यह बात तो ठीक है; लेकिन शिक्षा बेचने का कार्य करके पाप का भागी कैसे हुआ जा सकता है!
अन्त में सुश्री गाँधी ने कुछ स्थानीय लोगों को समझा-बुझाकर इस दम्पति के पास भेजा, जिन्होंने उनके दिमाग में यह बात डालने की कोशिश की कि यदि लक्ष्मी देवी शिक्षित हैं तो वे इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं! क्या उनका यह फ़र्ज नहीं बनता कि उन्हीं की तरह और बालिकाएँ भी पढ़ाई-लिखाई करें?
आखिरकार पत्थर पिघला। भगतजी ने स्वीकृति दी और लक्ष्मी देवी ने सरकारी बालिका विद्यालय में प्रधानाध्यापिका का पद-भार ग्रहण किया। समय की शिला पर नूतन इतिहास रचा गया। सौभाग्य से जिस मकान में लक्ष्मी देवी अपने पति के साथ रहती थीं, उसके सामने का मकान खाली था। उसे सरकार ने किराये पर लिया और सरकारी बालिका विद्यालय की शुरुआत हुई। लक्ष्मी देवी बहुत महत्त्वाकांक्षी नहीं थीं, बल्कि कुर्सी स्वयं उन तक–चलकर पहुँची थी। लेकिन एक बार वे उस कुर्सी पर बैठीं तो मानो वे ज़िन्दगी का मकसद समझ गयीं। शुरू-शुरू में वे ही प्रधानाध्यापिका थीं, वे ही शिक्षिका थीं, वे ही क्लर्क थीं। आगे चलकर स्कूल से पढ़-लिखकर जो छात्राएँ निकलीं, उन्ही में से कुछ ने उनकी सहायिका की ज़िम्मेदारी सँभाली। शिक्षा की जो पहली मशाल लक्ष्मी देवी ने जलायी, उसका विस्तार होता गया, मशाल से मशाल जलते गये। (आज वह विद्यालय विशाल महाविद्यालय के रूप में परिणत हो चुका है।)
लक्ष्मी देवी ने कभी पैसे के लिए शिक्षिका की नौकरी नहीं की, वे सेवा-भाव से अपना काम करती थीं। वे छात्राओं को अपने परिवार का सदस्य मानती थीं। न तो उन्हें कभी आकस्मिक अवकाश की जरूरत पड़ती थी और न ही उन्हें कभी अनावश्यक रूप से सरकारी कृपा का मोहताज होना पड़ा। समय-समय पर जब निरीक्षिका का स्कूल -प्रांगण में पदापर्ण होता तो स्कूल के निरीक्षण के बाद पूरा परिवार ही उनकी आवभगत में लग जाता था। उस जमाने में न तो एक्रेडिटेशन’ की समस्या थी और न ही अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की ललक। सहज भाव से विद्यादान की प्रक्रिया निरन्तर चलती रही,जिसकी पावनता और दिव्यता की सुगंध से पूरा बलिया शहर सुगंधित होता रहा।
बोर्ड की परीक्षा से पहले स्कूल की सभी छात्राएँ सत्यनारायण की कथा बड़े श्रद्धा भाव से सुनती थीं और परीक्षा के दिन रंगरेज के यहाँ की रँगी गयी साडियाँ पहनकर परीक्षा-भवन पहुँचतीं सबकी साड़ी का एक रंग, कोई भेद-भाव नहीं, कोई उँच-नीच नहीं; सब समरस, सब समान। श्रीमती लक्ष्मी देवी सप्ताह के सातों दिन काम करती थीं। छ: दिनों के लिए छात्राओं को पढ़ाने का कार्य-भार और रविवार तथा छुट्टी के लिए पत्र-लेखन का कार्य। पत्र टाइप भी नहीं होते थे, वे मोती-जैसे अक्षरों में ही सरकारी पत्र लिखतीं और सरकारी पत्रों के उत्तर तैयार करती थीं।
उन दिनों सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार का चलन नहीं था, लेकिन जब कभी वे बलिया की सड़कों पर चलती थीं, विशिष्ट-से विशिष्ट व्यक्ति भी उनका झुक-झुककर जिस श्रद्धा और सम्मान के साथ अभिवादन करते थे, उससे बढ़कर क्या कोई पुरस्कार हो सकता था!अवकाश-प्राप्ति के बाद लक्ष्मी देवी लगभग बीस वर्षों तक जीवित रहीं। हर महीने जब वे पेन्शन लेने के लिए सरकारी खजाना जातीं तो लोग उनके लिए रास्ता छोड़ दिया करते थे। उन्हें चूड़ियों का बड़ा शौक था, चुड़िहारिन उन्हें चूड़ी पहनाते-पहनाते पूछ बैठती थी– क्यों गुरुआइन, सरकार को तुमने कितना क़र्ज दिया है, जो अब तक वसूल रही हो।
दृष्टव्य : मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि लक्ष्मी देवी मेरी दादी थीं। उन्हीं की छत्रछात्रा में मुझे शिक्षा क्षेत्र का ककहरा सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
–डॉ. सुशीला गुप्ता